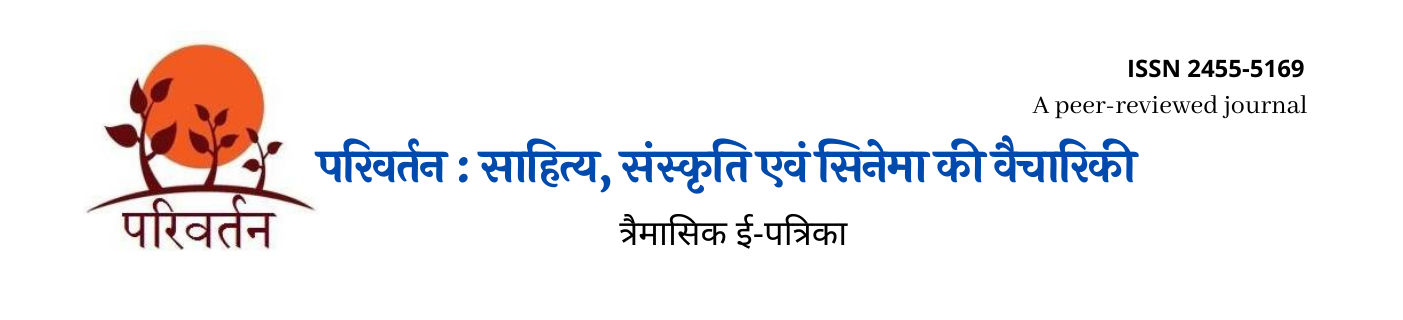साहित्य और समाज
*डॉ. मो. मजीद मिया
साहित्य, संस्कृत के सहित शब्द से बना है । साहित्य की उत्पति को संस्कृत साहित्य के आचार्यों ने “हितेन सह सहित तस्य भवः” की संज्ञा दी हैं जिसका अर्थ है कल्याणकारी भाव । साहित्य में जीवन एवं जगत का कल्याण होना अनिवार्य है क्योंकि इसमें ‘स:हित’ की भावना होती है, जो लोक जीवन के कल्याणकारी भाव का सम्पादन करता है । साहित्य के हर क्षेत्र में शब्द एवं अर्थ के योग के साथ-साथ लोक कल्याण की भावना का होना आवश्यक है । संस्कृत में सहित शब्द का दो अर्थ होता है, एक स्वभाव एवं दूसरा हितयुक्त अर्थात स्वभाव एवं हित का संतुलित रूप ही साहित्य है । साहित्य शब्द की व्युत्पति ने ही इसे लोगों के साथ जोड़ा है क्योंकि लोक साहित्य में लोक का अर्थ व्यापक एवं विस्तृत होता है । पर हम इसे साधारण अर्थ में समाज कह सकते हैं । यह संसार एक समाज है इसलिए साहित्य हमेशा समाज के हित की कामना करता है । यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी आत्मा । अगर देखा जाए तो साहित्य मनुष्य के मस्तिष्क से उत्पन्न होता है क्योंकि मनुष्य समाज का अभिन्न अंग है । जन्म से मृत्यु तक मनुष्य समाज से जुड़ा रहता है वह चाह कर भी समाज से अलग नहीं हो सकता है । उसका पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा तथा जीवन का निर्वाह समाज द्वारा ही होता है । मनुष्य समाज में रहकर अनेक प्रकार का अनुभव ग्रहण करता है एवं जब वह प्राप्त अनुभव को शब्द द्वारा अभिव्यक्त करता है तो वह साहित्य बन जाता है । और यही अभिव्यक्ति की शक्ति उस व्यक्ति को आगे चलकर साहित्यकार बना देती है । अतः जैसा समाज होता है वैसी ही साहित्यकार की रचना होती है और वैसे ही समाज की झलक उस साहित्य में देखने को मिलती है । साहित्य एवं समाज का संबंध युगों-युगों से देखा गया है दूसरे अर्थ में कहे तो साहित्य एवं समाज एक ही सिक्के के दो पहलू एवं एक दूसरे के पूरक भी हैं । साहित्य का सृजन समाज के लिए एवं समाज द्वारा ही होता है इसीलिए तो कहते हैं, साहित्य समाज का दर्पण है ।
साहित्य का सृजन मानव पटल में होता है क्योंकि यह एक कला है । यह कल्पना द्वारा पूर्ण होता है पर मानव कल्पना जीवन एवं जगत के अनुभव से प्राप्त करता है और वह अनुभव समाज से प्राप्त होता है । मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वह समाज से हर पल नए-नए अनुभव प्राप्त करता है एवं प्रत्येक अनुभवों को कल्पना के माध्यम द्वारा मनुष्य अपने कला को सृजित करता है इसी कारण प्रसिद्ध ग्रीस आचार्य एरिस टोटल ने साहित्य को जीवन एवं जगत का अनुकरण मानते थे । उनके मतानुसार साहित्य, जीवन एवं जगत की नकल है । जीवन एवं जगत में हो रहे घटनाओं को साहित्यकार अपने कला से नकल करता है एवं फिर से उसी समाज को लौटा देता है । साहित्यकार जिस समाज एवं वातावरण में रहते हैं उस समाज एवं वातावरण की सभी स्थितियाँ उसे हमेशा प्रभावित करती रहती हैं । साहित्यकार अपने रचना के जरिए जो भी समाज को देना चाहता है उसे वह बड़ी ही चतुराई से प्रस्तुत करता है एवं समाज के प्रत्येक सुख-दुख एवं समस्याओं का चित्र समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है । समाज का उत्थान-पतन, समाज की रीति-रिवाज, आस्था एवं संस्कृति स्पष्ट रूप से साहित्य में अपना प्रभाव डालता रहता है । साहित्य भी समाज के परिवर्तित स्वरूप के साथ बदलता रहता है । आधुनिक संदर्भ में भी साहित्य एवं समाज में परस्पर संबंध है । दोनों एक-दूसरे के लिए बने हैं । समाज में हो रही विसंगति एवं विकृति, प्रगति, उपलब्धि, अभाव, विषमता, समानता, सौंदर्यता, प्रेम, स्नेह, मातृत्व, देशप्रेम, विश्व बंधुत्व जैसे विविध पक्षों को साहित्यकार अपने साहित्य में सृजित करते हैं, जो नितांत लोकहित के लिए होता है । जिस प्रकार से समाज का प्रभाव साहित्य के ऊपर पड़ता है वैसे ही साहित्य का प्रभाव समाज पर भी पड़ता है । क्योंकि कवि अथवा लेखक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः वे लोग समाज को अपने नवीन विचार प्रदान करते रहते हैं । जब समाज में कोई समस्या आती है, समाजिक जीवन मूल्य का पतन होने लगता है तब साहित्य ही उसे दूर करने में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है । ऐसे समय में साहित्यकार समाज को नया रास्ता दिखाने का काम करता है । साहित्य के द्वारा राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों को देखा जाता है । आज विश्व में धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिकता, अलगाववाद तथा आतंकवाद गंभीर समस्याओं के विनाश के लिए साहित्य प्रयत्नशील है ।
साहित्यकार साहित्य का सृजन अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि समाज के उपयोग के लिए करता है । चाहे वह ऋग्वेदिक रचनाकार हो या वह वेदव्यास का भगवद् गीता हो या फिर बाल्मीकि का रामायण, शेक्सपियर का नाटक या एरिस्टोटल का काव्यशास्त्र ही हो सभी समाज के उपयोग एवं मार्ग दर्शन के लिए सृजित किए गए थे । हिन्दी साहित्य के लोककल्याणकारी कवि तुलसीदास ने समाज के कल्याण के लिए रामचरितमानस का सृजन किया यह उनके पहले श्लोक से ही स्पष्ट होता है । उसके बाद तो हिन्दी समाज में आमूल-चूल परिवर्तन आया । तुलसीदास रचित रामचरितमानस पढ़ने के लिए लोगों ने शिक्षार्जन करना शुरू किया, जिसके द्वारा हिन्दी समाज में शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ जिससे समाज में नवचेतना का प्रसार हुआ । इसी से यह कथन स्पष्ट होता है कि साहित्य की रचना लोक हित के लिए होती है ।
साहित्य सृजन के लिए साहित्यकार विषयवस्तु समाज के ही विभिन्न पक्षों से लेता है । चाहे वह ऐतिहासिक, पौराणिक या फिर सामाजिक विषयवस्तु क्यों न हो । इन सभी विषयवस्तु का समाज में ही सृजन होता है और इसी से साहित्यकार अपने दृष्टिकोण द्वारा समाज को उसके मूल्यांकन एवं विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करता है । प्राचीनकाल से आज तक साहित्यकार समाज के प्रत्येक परिवर्तनों को देखते आया है इसी से यह प्रमाणित होता है कि साहित्य का सृजन एवं समाज की भूमिका एक दूसरे के पूरक हैं ।
प्रत्येक समाज का अपना अलग रहन-सहन, परंपरा, संस्कृति , संस्कार और इतिहास है पर साहित्य इन सभी बातों को समेटकर प्रत्येक समाज की घटना को दूसरे समाज से आदान-प्रदान करता है । शेक्सपियर के नाटक, बालजाक की कहानी, लियो टोल्स्टोय की कहानियाँ, मेक्सिम गोर्की के उपन्यास, ओ. हेनरी के कहानी, वर्ल्ड हवितम्यान की कविताएं, शैली एवं किट्स की कविताएं, जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ, रवीन्द्रनाथ की कविताएं, प्रेमचंद के उपन्यास आदि इन सभी को देखने पर ही साहित्य एवं समाज के बीच का संबंध समझ में आता हैं । यह सभी साहित्य, सृजनाओं के द्वारा समाज के विभिन्न घटनाक्रम को लिखकर अनुभव एवं कल्पना द्वारा सृजन किया गया है । इसप्रकार से मानव सभ्यता के विकास में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका को देखा जा सकता है ।
साहित्य हमेशा मानव को सकारात्मक सोच के साथ-साथ समाज के लिए मनुष्य को कुछ करने की प्रेरणा प्रदान करता है । राष्ट्र-प्रेम की भावना जागृत कराता है और वसुधैव-कुटुम्बकम् की भावना विकसित कराता है । यह संसार मानव समाज का घर है और इसमें मानव समाज को किस प्रकार की भूमिका निर्वाह करने पर समाज का कल्याण होगा यही सीख देना साहित्य का काम है । अपने साहित्य सृजन में विषय-वस्तु के अतिरिक्त पात्रों को भी लेखक समाज से ही चुनता है । समाज से लिया गया पात्र किसी विशेष समाज का प्रतिनिधित्व करने के साथ-साथ कतिपय पात्र विश्वजनित बन जाता है, जो समाज को कुछ न कुछ संदेश दे रहा होता है । किसी भी समाज को निकट से पहचानने का जरिया ही साहित्य है । प्राचीन भारत के वैभवपूर्ण संस्कृति को वेद, पुराण, रामायण, महाभारत जैसे साहित्यक रचना ने ही पहचान दी है, तो ग्रीस के सभ्यता को ओडिसी एवं इलियट जैसे ग्रन्थों ने पहचान देने का काम किया है । समाज एवं साहित्य मानव सभ्यता के वह पक्ष हैं जो एक दूसरे के बिना पूरे नहीं हो सकते । अतः कोई एक पक्ष कमजोर होने पर उस समाज के उत्थान एवं प्रगति के क्रम में बाधा आ सकती है ।
डॉ. मजीद मिया, (सहायक अध्यापक) यस एम् यस एन, हिंदी हाई स्कूल, ग्राम.+पोस्ट बागडोगरा, जिला दार्जिलिंग (प.ब.) -734014, मोब.-9733153487 मेल- Khan.mazid13@yahoo.com