अज्ञेय की काव्य संवेदना और असाध्यवीणा
रामचन्द्र पाण्डेय
प्रयोगवादी कवियों में अग्रगण्य सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन अज्ञेय शब्दों में नये अर्थ का अनुसन्धान करने वाले बल्कि यूँ कहें कि अर्थों मे नयी चेतना की जीवन्त झंकृति भरने वाले स्वर साधक रचनाकार हैं । उनकी रचनाओं का दायरा बहुत विस्तीर्ण है जिसमें प्रमुखतया अपने देश की माटी की सोंधी सी गन्ध सर्वत्र व्याप्त है। एक ओर उनके काव्य में आशा की ज्योति का और अदम्य उत्साह का प्रवाह है तो दूसरी ओर जीवनजन्य अनुभवों की व्यापकता भी चित्रित है। एक ओर वे मृत होते हुए शब्दों में नयी जान फूंक देते हैं तो दूसरी ओर शब्दों को एक नवीन अर्थ भी प्रदान करते चलते हैं। वे सच्चे अर्थों में शब्द-संधित्सु साहित्यकार हैं। पं0 विद्यानिवास मिश्र के शब्दों में- ‘‘वे शब्द की खोज के लिए परेशान नहीं हैं, परिचित शब्दों मे नये अर्थ की खोज करना चाहते हैं, परिचित प्रत्ययों में नये प्रत्यय की खोज करना चाहते हैं। वे परायें देशों की बेदर्द हवाओं और उनके नंगे अंधेरे से खिन्न विकल और संत्रस्त हैं, केवल अपनी छोटी सी ज्योति से आश्वस्त हैं क्योंकि यह ज्योति उनकी अपनी है, अपने प्रयत्न से अर्जित है, अपने अनुभवों से दीप्त है”।[1]
वस्तुतः वे एक साथ जीवन में अर्थ का सन्धान करने वाले रचनाकार हैं और रचना में अर्थ का अनुसंधान करने वाले आलोचक भी और साथ ही साथ वे आधुनिक भारतीय चिन्तकों की उस शीर्षस्थ श्रेणी में भी परिगणित हैं जो अपनी साहित्य साधना से वास्तविक जीवन में समरसता की वीणा के स्वरों की मधुर झंकृति सुनना चाहता है और उनकी इसी साधना की परिणिति है ‘असाध्यवीणा‘। असाध्यवीणा वस्तुतः समष्टि में व्यष्टि के विलयन का विश्व-वीणा के स्वर की झंकृति में अपने अहम् के बलिदान की मानवीय रचनात्मकता की अदम्य जीवनी शक्ति का जीवन्त दस्तावेज है। तभी तो केशकम्बली प्रियंवद के आगमन पर राजा के विश्वस्त कण्ठ से यह स्वतः प्रस्फुटित होता है कि-
‘‘कृतकृत्य हुआ मैं तात! पधारे आप।
भरोसा है अब मुझको
साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी”।[2]
इन पंक्तियों के माध्यम से अज्ञेय यह कहना चाहते हैं कि जनसमुदाय ऐसे व्यक्तियों पर ही विश्वास कर सकता है जिसने निरन्तर साधना के द्वारा अपने अहं का विसर्जन कर दिया हो, स्वत्व का विलयन कर दिया हो, ऐसा व्यक्ति ही, ऐसा साधक ही विश्व-वीणा में मानवीय स्वरों की, समरसता की झंकृति को भर सकता है, उसकी छुअन से ही विश्व-वीणा की रागिनी प्रकट हो सकती है। अब तक के सारे कलावन्तों की असफलता का कारण भी यही था कि उनमें अकारण दर्प और अहंकार विद्यमान था। राजा का यह कथन इस बात का प्रबल साक्ष्य भी प्रस्तुत करता है-
“मेरे हार गये सब जाने-माने कलावन्त,
सब की विद्या हो गयी अकारण, दर्पचूरः
कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका।
अब यह असाध्यवीणा ही ख्यात हो गयी।
पर मेरा अब भी है विश्वास
कृच्छ् तप बज्रकीर्ति का व्यर्थ नहीं था।
वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी
इसे जब सच्चा स्वरसिद्ध गोद में लेगा”।[3]
अज्ञेय का मानना है कि कोई कलाकार सच्चे अर्थों में कलाकार तभी होगा जब उसने अपनी कला में अपने व्यक्तित्व को घोल दिया हो, वह अपनी साधना में इस प्रकार डूब जाय कि साध्य और साधक का भेद ही मिट जाय और बचे तो सिर्फ साधना जो अपने ही प्रकाश से भाष्यमान होकर जगत् में फैली हुई कालिमा को भस्मीभूत कर सके।
असाध्यवीणा का नायक प्रियंवद भी अपने व्यक्तित्व को अपनी साधना में घोलकर इस प्रकार एकतान हो जाता है कि उसके स्वत्व का कहीं पता ही नहीं चलता। वह जानता है कि साधना समर्पण माँगती है और समर्पित व्यक्ति ही अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने में समर्थ होता है। हिन्दी के भक्तिकालीन कवियों ने भी परमात्मा के चिन्तन में अपने आपको इस प्रकार संलग्न करने की शिक्षा दी कि स्वयं ‘आत्म‘ में ही ‘परमात्मभाव‘ जाग उठे- ‘जानत तुम्हहिं तुम्हहिं होइ जाई, मानुष प्रेम भयऊ बैकुण्ठी, हरिजन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होय‘ जैसी पंक्तियाँ इस बात की साक्षी हैं। प्रियंवद भी तो वीणा से यही निवेदन करता है-
‘‘मैं नहीं, नहीं! मैं कहीं नहीं!/ओ रे तरु! ओ वन!
ओ स्वर-सम्भार?/नादमय संस्कृति!/ओ रस प्लावन!
मुझे क्षमाकर- भूल अकिंचनता को मेरी-
मुझे ओट दे-ढँक ले- छा ले-/ओ शरण्य!
मेरे गूंगेपन को तेरे सोये स्वर-सागर का ज्वार डुबा ले!
आ मुझे भुला,/तू उतर बीन के तारों में
अपने से गा/अपने को गा-
अपने खग कुल को मुखरित कर
अपनी छाया में पले मृगों की चैकडि़यों को ताल बाँध,
अपनी छाया तप, वृष्टि-पवन, पल्लव-कुसुमन की लय पर
अपने जीवन-संचय को कर छन्दयुक्त,
अपनी प्रज्ञा को वाणी दे!/तू गा, तू गा-
तू सन्निधि पा- तू खो/ तू आ- तू हो- तू गा! तू गा”![4]
और इसी का परिणाम है कि प्रियंवद सदियों से न साधी गयी वीणा में एक ऐसे स्वर को गुंजायमान बना देता है जो सबको अपना लगता है-
‘‘किसी एक को नयी वधू की सहमी-सी पायल ध्वनि
किसी दूसरे को शिशु की किलकारी।
किसी एक को जाल फँसी मछली की तड़पन-
एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिडि़या की”।[5]
क्या ये पंक्तियाँ कामायनीकार जयशंकर प्रसाद की इन पंक्तियों की याद नहीं दिलाती-
‘‘समरस थे जड़ या चेतन सुन्दर साकार बना था
चेतनता एक विलसती आनन्द अखण्ड घना था।‘‘
वस्तुतः ‘जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी‘ कलावन्त विश्व-वीणा में ऐसे ही स्वरों की झंकृति भरना चाहता है जिससे सभी सुखी, सम्पन्न और आनन्दपूरित हों। इन्हीं अर्थों में अज्ञेय सच्चे स्वर साधक से सच्चे जीवन साधक रचनाकार बन जाते हैं। खासियत यह कि सारी ऊर्जस्वित साधना के बावजूद श्रेय स्वयं न लेकर उसी सर्वशक्तिमान, समष्टि के आराध्य को समर्पित कर देता है-
‘‘श्रेय नहीं कुछ मेराः
मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में-
वीणा के माध्यम से अपने को मैनें
सब कुछ को सौप दिया था”।[6]
यही समष्टिभाव की आराधना और विश्व-वीणा में अपने स्वर को विलीन कर देना ही ‘असाध्यवीणा‘ को साध्य बना देता है और अज्ञेय को जीवन के विविध अनुभवों की वास्तविकता का साक्षी भी। अस्तु वे एक सच्चे जीवन-साधक रचनाकार बन जाते हैं।
| संपर्क: शोधछात्र, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश |
[1] मिश्र, विद्यानिवास, अज्ञेय प्रतिनिधि कविताएँ एवं जीवन परिचय, पृ0सं0 32
[2] मिश्र, विद्यानिवास, अज्ञेय प्रतिनिधि कविताएँ एवं जीवन परिचय, पृ0सं0 94
[3] मिश्र, विद्यानिवास, अज्ञेय प्रतिनिधि कविताएँ एवं जीवन परिचय, पृ0सं0 95
[4] मिश्र, विद्यानिवास, अज्ञेय प्रतिनिधि कविताएँ एवं जीवन परिचय, पृ0सं0 101-102
[5] मिश्र, विद्यानिवास, अज्ञेय प्रतिनिधि कविताएँ एवं जीवन परिचय, पृ0सं0 104
[6]मिश्र, विद्यानिवास, अज्ञेय प्रतिनिधि कविताएँ एवं जीवन परिचय पृ0सं0 105
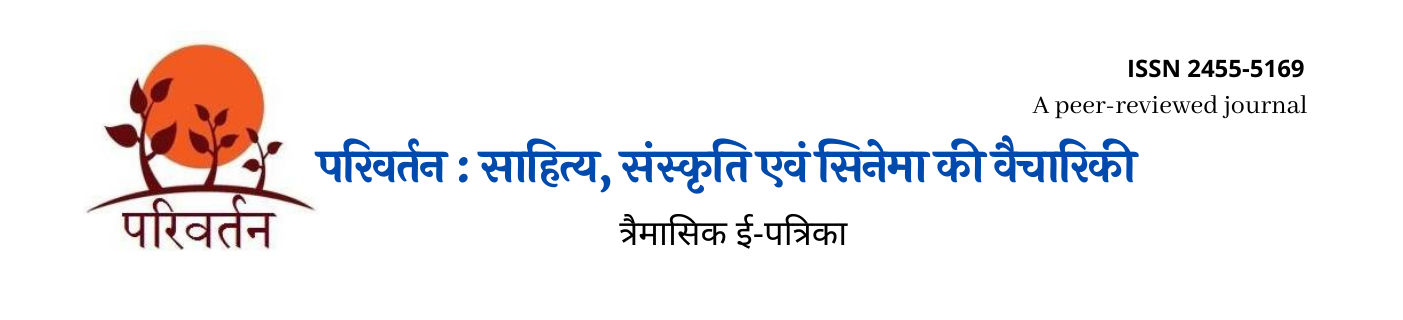

Leave a Reply