ईशावास्य : रामचरित मानस का आधार दर्शन
*प्रभुदयाल मिश्र
तुलसीकृत रामचरित मानस सगुण राम के चरित-गायन ग्रन्थ के रूप में जगत प्रसिद्ध है । इसके दार्शनिक आधारों की खोज करते हुए इसे विशिष्टाद्वैत परक रचना माना जाता है । किन्तु हम तुलसी के इस प्रतिज्ञा कथन को संभवतः कैसे भी विस्मृत नहीं कर सकते कि रामायण ‘नानापुराण निगमागम सम्मतम्’ है । अर्थात् मानस वेद-मत पर आधारित है । किन्तु वैदिक साहित्य तो अपार है अतः स्वभाविक रूप से हमें वेद के सार स्वरूप की पहचान करनी आवश्यक है । इसके लिए यजुर्वेद का अंतिम चालीसवां अध्याय (जो यथावत् ईशावास्योपनिषद् है) का आश्रय लेना सर्वथा उचित है । वस्तुतः इसके १८ मंत्र भारतीय मनीषा और वैदिक दर्शन के सार सर्वस्व हैं । हम यहाँ इन मन्त्रों के संकेत का आधार लेकर रामचरित मानस के सन्देश की विश्वजनीनता पर विचार कर रहे हैं ।
ईशावास्य का पहला मंत्र है –
ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किन्च्जगत्यां जगत्
तेन त्यक्तेन भुन्जीथः मा गृधः कस्यस्वित्धनम् ।
इस मंत्र के प्रथम भाग में ईश्वर की सर्वव्यापकता की उद्घोषणा है । संसार का प्रत्येक चेतन-अचेतन जीव अथवा पदार्थ ईश्वर से आच्छादित, आवेष्ठित है । यह दृष्टि संसार में भेद के स्थान पर सम्पूर्ण अभेदता की पोषक है । इसे गीता में कृष्ण ने यह कहते हुए और अधिक स्पष्ट किया है कि ‘मुझ एक धागे में सम्पूर्ण संसार मणि रूप में’ ( मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मनिगणा इव ७/७ ) पिरोया हुआ है । गोस्वामी तुलसीदास ने इस सूत्र को मानस के वंदना-प्रसंग में सभी को – सज्जन और असज्जन सहित, पूरी तरह से प्रणाम करते हुए स्वीकार किया है-
सीय राममय सब जग जानी , करउं प्रनाम जोरि जुग पानी (बाल. ७ घ २ )
सनातन भारतीय दर्शन ईश्वर को दूरदेशीय नहीं मानता । वह सृष्टि का कारण और निमित्त दोनों तो है ही, सदा कार्य रूप में भी विद्यमान है । वह कुम्हार ही नहीं, घडा बन जाने वाली मिट्टी और स्वयं घडा भी है । ऐसे ईश्वर की खोज में किसी को भी कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है । अन्यथा एक ईश्वर की खोज तो सदा अपूर्ण ही रही है और अपूर्ण ही रहने वाली है ।
ईश्वर की पहचान में ईश्वर के निर्गुण और सगुण रूप की दो धाराएं सर्व व्यापक हैं । इनके अनुयायी इनमें परस्पर इतनी दूरी भी उत्पन्न करते रहे हैं कि इनका एक व्यवहारिक समन्वय प्रायः सुगम प्रतीत नहीं रहा । यह मानना स्वाभाविक ही है कि ईश्वर अपनी अव्यक्त अवस्था में सर्वशक्तिमान हो सकता है, अतः यदि वह अवतार भी लेता है तो एक सीमा ही स्वीकार करता है तथा इस प्रकार उसका आचरण और कृत्य प्रायः मनुष्यों के ही समान हो जाते हैं जो कभी-कभी आदर्श होकर समालोच्य भी होते हैं ।
भारतीय द्रष्टा ऋषियों ने इस सत्य को निकट से पहचाना है । राम और कृष्ण के पूर्ण अवतार का निदर्शन कराने वाले वाल्मीकि और व्यास अपनी रामायण और भागवत में इन दार्शनिक प्रश्नों का समाधान खोजते हैं । श्रीमद्भागवत के पहले ही श्लोक में भगवान वेदव्यास उस ‘परम सत्य’ ( सर्वशक्तिमान अव्यक्त ईश्वर द्वारा सृष्टि संरचना प्रक्रिया का उपक्रम) के सगुण अनुसंधान (सत्यं परम धीमहि) का प्रतिज्ञा कथन करते हैं – जिससे इस संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय है, जिसके सम्बन्ध में विद्वान् दिग्भ्रमित होते हैं किन्तु वह स्वयं ज्ञान से प्रकाशित रहता है । श्रीकृष्ण के ब्रज में विहार, मथुरा में युद्ध, द्वारिका में विवाह और कुरुक्षेत्र में युद्ध दीक्षा के चरित्र की वेदान्त की जिस भूमिका में व्यासजी प्रतिष्ठा करते हैं ठीक वही स्थापना गोस्वामी तुलसीदास की भी रामकथा की पृष्ठभूमि में है-
यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा
यत्सत्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथाहेर्भ्रमः
यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तीर्षावताम्
वंदेऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् । बाल. ६
यहाँ इतना कहना पर्याप्त है कि रामचरित मानस की सरंचना के दार्शनिक पक्ष की निष्पत्ति में तुलसी वेदव्यास की श्रीमद्भागवत के अधिक निकट हैं जबकि महाकाव्य के विधान रूप में इसमें उन्होंने वाल्मीकि की रामायण से प्रेरणा ली है । और चूंकि दर्शन की यह सनातन परम्परा वेदान्त परक है अतः इसमें ईशावास्य के आधार दर्शन का समावेश प्रचुरता से हुआ है ।
हम अब ईशावास्य के पहले मंत्र के दूसरे भाग पर आते हैं । इसमें कहा गया है कि ‘सभी वस्तुओं को परमात्मा को अर्पित करने के बाद ही उनका उपभोग उचित है । ‘लोभ कदापि वांछनीय नहीं, भला, यह धन यहाँ किसका है !’ इस सूत्र में मनुष्य के लिए आवश्यक यज्ञ, त्याग, अपरिग्रह, समर्पण, निष्कामता, निर्लोभ, समता, निर्भेदता और समभाव आदि सभी वांछनीय गुण समाविष्ट हैं । गीता में श्री कृष्ण ने ऐसे एक कर्मयोगी राजा जनक का उदाहरण दिया जिन्हें संसिद्धि प्राप्त हुई । जब हम मानस के कथानक पर दृष्टिपात करते हैं तो इसमें एक चरित्र राजा प्रतापभानु ऐसा है जिसके बारे में तुलसी ने लिखा-
हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप बिबेकी परम सुजाना
करइ जे धरम करम मन बानी, बासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी । बाल. १५५/१
यह अपने आप में कितना बड़ा आश्चर्य है कि इस ‘कर्मयोगी’ राजा को अन्ततः रावण बनना पड़ता है । इसका क्या कारण है ? इसका उत्तर उपनिषद के इस दूसरे चरण में मिल जाता है । इस राजा ने लोभ का परित्याग नहीं किया और उसमें एक अत्यंत प्रबल आकांक्षा उत्पन्न हो गयी –
ज़रा मरन दुःख रहित तनु समर जिते जनि कोउ
एकछत्र रिपुहीन महि राज कलप सत होउ । (बाल १६४)
उपनिषद् के लोभ परित्याग के सन्देश का इससे महत्तर विस्तार अन्यत्र देखा जाना कठिन है । त्याग की इतनी महत्ता प्रतिपादित कर ईशावास्य के दूसरे मंत्र का सन्देश यही कि वास्तव में यह दर्शन ‘कर्म’ का है, त्याग का नहीं, सही कर्म की इससे भिन्न स्थिति नहीं है । मनुष्य को अपनी सम्पूर्ण १०० वर्ष की इच्छित आयु इसी रीति से व्यतीत करनी है । इससे भिन्न तो केवल अंध तमस का लोक ही है जहां ‘आत्म-घाती’ लोग पहुंचा करते हैं !
रामचरित मानस में जैसे विभीषण और रावण के व्यक्तित्व इन दो धाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, विभीषण को भगवान अंत में यही आदेश देते है- ‘करेहु कल्प भर राजु तुम्ह, मोहि सुमिरेहु मन माहिं’ (उत्.११६ घ) जबकि रावण की जीवन शैली का निदर्शन वे इन शब्दों में करते हैं- ‘कहुं महिष मानुस धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहीँ’ (सुन्द.२/३ )
ईशावास्य के ४ से लेकर ८ तक के पांच मंत्र ईश्वर की ‘निखिल धर्म विरुद्ध आश्रयी’ विशेषताओं का निरूपण करते हैं । इसके अनुसार ईश्वर देवताओं और मन से भी तीव्रतर गतिशील, भीतर और बाहर समान रूप से समुपस्थित, अकाय, शुद्ध, कवि, मनीषी, परिभू और स्वयम्भू है । उसे इस रूप में देखने वाले मैं और तू जैसा भेद नहीं रखते । अतः उनके लिए जीवन में किसी प्रकार का शोक या मोह उत्पन्न नहीं होता । मानस में तुलसी ने ईश्वर की इन विशेषताओं का अनेकशः वर्णन किया है । वह –‘बिनु पग चलइ सुनइ बिनु काना, कर बिनु करम करइ विधि नाना’ ( बाल. ११७ ३-४) है तथा उसे इस रूप में देखने वाले यही जानते हैं कि – ‘मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत’ ( किष्कि. ३)
ईशावास्य में आगे विद्या और अविद्या तथा सम्भूति और असम्भूति की त्रयी बहुत गहन अध्यात्म दर्शन का निदर्शन करती हैं । वेद के ऋषि का इसमें यह कथन है कि अविद्या के उपासक अंध तमस में प्रवेश करते हैं किन्तु विद्या में रत कहीं अधिक गहरे तमस में भटक जाते हैं । इसी तरह असम्भूति के उपासक भी जहां अंध तम में रहते हैं वहीं संभूति में रत और गहरे अन्धकार में भटकते हैं । अतः ऋषि का परामर्श यहाँ यह है कि इन दोनों स्थितियों की जब व्यक्ति को ठीक समझ हो जाती है तो वह अविद्या/असम्भूति से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर विद्या/सम्भूति के द्वारा अमृतत्व में प्रतिष्ठित होता है ।
वैदिक दर्शन के व्याख्याकारों ने इन सिद्धांतों की विस्तृत और गहन व्याख्या की है । सामान्यतया इन्हें भौतिक और अध्यात्म तथा व्यक्त और अव्यक्त धाराओं का प्रतीकार्थी कहा जा सकता है । तुलसी ने भी सृष्टि संरचना में प्रधान ईश्वरीय सामर्थ्य ‘माया’ को ‘विद्या अपर अविद्या दोऊ’ (बाल १४/२) भेद वाला माना है । संक्षेपतः यहाँ यह कहना भी आवश्यक है कि उपनिषद् में ‘विद्या’ और ‘सम्भूति’ के लिए ‘रत’ विशेषण प्रयुक्त है । इसका अर्थ यह हुआ कि ज्ञान के प्रति आसक्ति होने पर वह भी बंधनकारी ही होता है । तुलसीदास जी जैसे सार रूप में समझा देते हैं-
ज्ञान मान जहं एकउ नाहीं, देख ब्रह्म समान जग माहीं (आर. १४/४)
औपनिषदिक शब्दावली में ही तुलसी ‘ज्ञान पथ’ की तुलना कृपाण की धार (उत.११८/१) से करते हैं । अर्थात ज्ञान के मार्ग में भटकने के पूरे अवसर हैं । किन्तु जब ईश्वर की सर्वव्यापकता किसी की अनुभूति बन जाती है तो यहीं मृत्यु से संतरण के बाद उसकी अमृत में प्रतिष्ठा होती है ।
उपनिषद् का मंत्र १५ अन्यथा भी बहुत ख्यात है । इसके अनुसार सत्य का मुख स्वर्ण के ढक्कन में छुपा हुआ है । अतः ऋषि सूर्य से प्रर्थना करता है कि वह सत्य और धर्म के जिज्ञासु को उसे देखने के लिए खोलें । अगले मंत्र सोलह में पुनः सूर्य से अपने रश्मि जाल को समेट लेने की प्रार्थना की गयी है जिससे अंततः वह (ऋषि) यह समझ सके कि जो परमात्मा उसमें है वह स्वयं भी वही है ।
वेद और लोक में संसिद्ध और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र (ऋग्वेद ३/६२/१०) में सविता देव से भी ऋषि की प्रार्थना अपनी बुद्धि को स्वयं प्रकाश की ओर ले जाने की है । मानस के उत्तरकाण्ड में आत्मसाक्षात्कार की इस अवस्था को तुलसीदासजी ने इस प्रकार प्रकट किया है-
सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीपसिखा सोइ परम प्रचंडा
आतम अनुभव सुख सो सुप्रकासा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा । (उत्त. /११७/१)
उपनिषद् का मंत्र क्रमांक १७ पञ्चतत्वों से निर्मित नश्वर देह के नाश के अवसर पर कर्तव्य कर्म का स्मरण कराता है । गीता के आठवें अध्याय में भी अर्जुन श्री कृष्ण से देहांतरण की साधना प्रदान करने का अनुरोध करते हैं । वेद के द्रष्टा ऋषि के द्वारा ऐसे प्रस्थान कामी को ‘क्रतो’ और ‘कृतं’ के स्मरण का निर्देश किया गया है । कुछ भाष्यकारों के अनुसार इसमें ईश्वर की कृपा और अपने कर्मों के स्मरण का सन्देश है । जिस तरह गीता मृत्युकामी को भगवान के ‘अनुस्मरण’ का परामर्श देती है, रामायण के अनुसार बाली अपनी मृत्यु शैया पर इस सम्पूर्ण दर्शन को बड़ी कुशलता से प्रकट करता है-
जन्म जन्म मुनि जतन कराहीं, अंत राम कहि आवत नाहीं
मम लोचन गोचर सोइ आवा’ (कि. ९/३)
ईशावास्योपनिषद् का अंतिम अठारहवां मंत्र अग्नि को समर्पित है । सब जानते हैं कि अग्नि वेद के प्रधान देवता हैं । ऋग्वेद में जहां इन्द्र के सम्बन्ध में सर्वाधिक लगभग २५० सूक्त हैं वहीं दूसरे क्रम में अग्नि के सूक्तों की संख्या लगभग २०० है । अग्नि अपनी प्रखरता में किसी वक्रता या प्रच्छन्नता को स्वीकार नहीं करता । वास्तविक समर्पण और स्वीकार की क्रिया की दीक्षा अग्नि ही देता है । अतः इस मंत्र में ऋषि अग्नि से प्रार्थना करता है कि ‘हे अग्नि हमें सन्मार्ग पर ऊपर ले चलो, तुम्हें सभी कुछ ज्ञात है, हमारे कुटिल कर्मों का दहन कर दो, हां बार-बार यहाँ यही प्रार्थना कर रहे हैं ।’ मानस के सन्दर्भ में हम यहाँ सीता की अग्नि-परीक्षा का स्मरण करना चाहते हैं । रावण विजय के पश्चात् राम जब सीता को इस आशय का संकेत देते हैं, तो-
लछमन होउ धरम के नेगी पावक प्रकट करहु तुम वेगी । (६/१०८/१)
श्रीखंड सम पावक प्रबेश कियो सुमिर प्रभु मैथिली । (६/१०८/१ (छंद)
इस प्रकार विचार करते हुए यही प्रतीत होता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस में ईशावास्योपनिषद् का न कवल सम्पूर्ण दार्शनिक आधार ग्रहण किया है अपितु उन्होंने अपने इतिवृत्त में भी उन सूत्रों को सहेजते हुए उन्हें व्यवहारिक और वैश्विक आधार प्रदान किया है ।
संपर्क : ३५, ईडन गार्डन, चुनाभट्टी, कोलार रोड भोपाल, १६
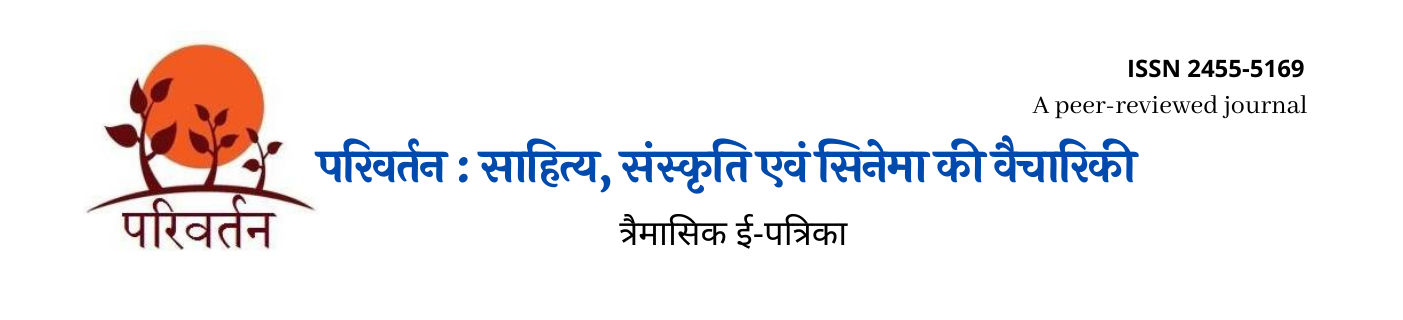

A WordPress Commenter
Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.